भारत, इज़रायल, फ़िलिस्तीन नए समीकरण नई एकजुटताओं की मांग करते हैं
Topics
इज़राइल और फ़िलिस्तीन के प्रति भारत का रुख़ नाटकीय रूप से बदल गया है। कभी साम्राज्यवाद-विरोधी एकजुटता पर आधारित, नई दिल्ली अब इज़राइल के साथ बढ़ते सैन्य, आर्थिक और वैचारिक संबंधों के साथ-साथ बयानबाज़ी को भी संतुलित कर रही है। यह विस्तृत लेख ऐतिहासिक घटनाक्रम का पता लगाता है, क्षेत्रीय गतिशीलता की पड़ताल करता है, और इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे हिंदुत्व भारत की विदेश नीति और घरेलू प्रतिक्रियाओं को नया रूप दे रहा है।
Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
यह तथ्य कि इज़रायल के तीन प्रबल सहयोगी – ब्रिटेन, फ़्रांस और कनाडा – ग़ज़ा में उसके नरसंहारक अभियान के कारण उसके खिलाफ़ ‘ठोस कार्यवाही’ की धमकी देते हैं, जबकि भारत हथियार और ड्रोन की आपूर्ति जारी रखता है, केवल उन्हीं को आश्चर्यचकित करेगा जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद से लगातार भारतीय सरकारों द्वारा फ़िलिस्तीनी मुद्दे को लेकर अटूट समर्थन की औपचारिक बयानबाज़ियों को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया है।
जहाँ भारत ने नए उत्तर-औपनिवेशिक राज्य के रूप में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के हित में गहराई से महसूस की गई साम्राज्यवाद-विरोधी एकजुटता की भावना से शुरुआत की, वहीं उसने आरंभ से ही ज़ायोनवादी सत्ता की आंशिक मान्यता और कभी-कभी उसकी वकालत के बीजों को भी सँजोए रखा। साथ ही पश्चिम के साथ संबंध सुधारने, या मध्य-पूर्व के देशों में अधिक प्रभाव फैलाकर तथा उनसे समर्थन प्राप्त करके पाकिस्तान का मुकाबला करने की कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी सक्रिय रहीं, जो समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण हो गईं। मोदी सरकार के आगमन से काफी पहले, सोवियत संघ के पतन और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद, यह ढुलमुल संबंध इज़रायल के साथ अधिक खुले सहयोग में बदल गया। हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में नव-उदारवादी हिंदुत्व के बढ़ते कदमों के साथ इज़रायल के अपराधों की प्रतीकात्मक निंदा भी तेज़ी से पुरानी बात होती जा रही है, क्योंकि भारतीय और ज़ायोनी राज्यों के बीच अधिकाधिक वैचारिक जुड़ाव और आर्थिक व सैन्य सहयोग बढ़ रहा है।
निस्संदेह इस पश्चिमी तिकड़ी ने भी इज़रायल को भौतिक सहायता देना बंद नहीं किया है – जिसमें हथियारों की बिक्री शामिल है। लेकिन औपचारिक बयानों में कितना बड़ा अंतर आ गया है! 19 मई 2025 को जारी उनके संयुक्त बयान में इज़रायल पर अंतर्राष्ट्रीय क़ानून तोड़ने का आरोप तो नहीं लगाया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया कि ग़ाज़ा में इज़रायल की सैन्य कार्रवाई ‘पूरी तरह असंगत’ है और ‘हम उस वक्त चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे जब नेतन्याहू सरकार इन घिनौनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है।’ इसके अलावा, उनके बयान आगे कहता है कि ‘हम आगे की कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे, जिसमें लक्षित पाबंदियां भी शामिल हैं’ (Gov.uk 2025)।
17 जनवरी 2025 को इज़रायल ने हमास के साथ युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन 18 मार्च 2025 को उसने उस युद्धविराम को तोड़ते हुए हवाई हमले फिर से शुरू किए। नेतन्याहू ने कुछ घंटे बाद घोषणा की कि इज़रायल ने ‘पूरी ताक़त से युद्ध फिर से शुरू कर दिया है।’ दो दिन बाद आए भारत के आधिकारिक बयान में हमास के साथ इज़रायली समझौते के उल्लंघन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया और, ढेर सारी प्रभावहीन घोषणाओं के अलावा, अत्यंत सावधानी बरती गई कि कहीं ऐसा कुछ न निकल जाए जिसमें नाम लेकर इज़रायल की आलोचना (निंदा की बात तो छोड़ ही दीजिए) हो। ग़ाज़ा में क्या हो रहा है, इसका सबसे क़रीबी उल्लेख यह था कि ‘भारत ने जनवरी 2025 के बंधकों की रिहाई और ग़ाज़ा में युद्धविराम के समझौते का स्वागत किया। भारत ने मानवीय सहायता की सुरक्षित, समयानुकूल और निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है’ (विदेश मंत्रालय 2025)। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने इस वर्ष 30 अप्रैल को सुरक्षा परिषद की बहस में फिर से युद्धविराम की आवश्यकता, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की अबाध आपूर्ति के बारे में वही घिसे-पिटे बयान दोहराए, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि (हालाँकि 20 महीने बीत चुके हैं) 7 अक्टूबर 2023 के आतंकवादी हमले की फिर से निंदा करें। मोदी सरकार के घिनौने नैतिक दोहरे मानदंडों को जो चीज़ उजागर करती है, वह यह है कि तब से अब तक उसने कभी भी ग़ाज़ा में इज़रायल की किसी भी कार्रवाई को आतंकवादी कृत्य नहीं कहा; नरसंहारक कहने की बात तो छोड़ दीजिए, उसने न ही नागरिकों की सामूहिक हत्याओं को आतंकवादी अभियान कहा। हालाँकि सही है कि भारत ने नरसंहार सम्मेलन (Genocide Convention) पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे अनुमोदित भी किया है, लेकिन मोदी सरकार ने दक्षिण अफ़्रीका की पहल पर, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (जिसका भारत सदस्य है) से ग़ाज़ा में इज़रायल के नरसंहार की जाँच करने और उस पर निर्णय लेने का आह्वान किया, न तो स्वीकृति दी और न ही उस पर टिप्पणी की।
इतना ही नहीं। कनाडा, अमेरिका और जर्मनी सहित कई यूरोपीय देशों में फ़िलिस्तीनियों और ख़ास तौर पर ग़ाज़ावासियों के समर्थन में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रदर्शन हुए हैं। विश्व के तथाकथित सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में, नागरिक समाज की प्रतिक्रिया तुलना के लिहाज़ से कहीं अधिक सीमित रही है। इसका एक कारण किसी न किसी रूप में दमन का भय है—भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों और दिल्ली में जब भी कार्रवाई हुई तो पुलिस ने उन पर रोक लगा दिया। यह हिंदू राष्ट्रवादी ताक़तों (या हिंदुत्व) द्वारा फ़िलिस्तीन को तथाकथित रूप से ‘हिंदू-विरोधी’ और इसलिए ‘राष्ट्र-विरोधी’ मुद्दा बताकर इस्लामोफ़ोबिया पनपाने में उनकी सफलता का भी प्रमाण है। वर्तमान लोकसभा में मौजूद लगभग 41 दलों में से 31 ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इज़राइल-ग़ाज़ा के बीच जो हो रहा है, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। क्यों कोई विदेश नीति का मुद्दा उठाने की ज़हमत उठाए, ख़ासकर ऐसा मुद्दा जिसे बहुसंख्यक हिंदू समुदाय और मतदाताओं के कई हिस्से ‘मुस्लिम तुष्टीकरण’ मान सकते हैं। यह तथ्य कि यह नजरिया अधिकांश राजनीतिक समूहों में मौजूद है, अपने आप में इस बात का संकेत है कि हिंदुत्व की भावनाएँ नागरिक समाज में कितनी व्यापक और गहरी पैठ बना चुकी हैं। यहाँ तक कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में भी, जैसे कांग्रेस शासित कर्नाटक में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में सार्वजनिक प्रदर्शन करने के प्रयासों को सीमित कर दिया गया, भले ही इसकी बर्बरता भाजपा शासित उत्तर प्रदेश (जो आबादी के लिहाज़ से दुनिया के देशों में पाँचवें स्थान पर आता है) जैसी नहीं रही हो। (द हिंदू 2024; हुसैन और माइक 2024)।
उस भारत का क्या हुआ जो दक्षिण का एक अग्रणी देश माना जाता था, और जो फ़िलिस्तीनी हितों के लिए अपने कथित दीर्घकालिक और निरंतर समर्थन के लिए जाना जाता था? हाँ, अतीत में भारत ने फ़िलिस्तीनी हितों का समर्थन किया था, लेकिन वह कभी भी उतना सुसंगत या सिद्धांतनिष्ठ नहीं रहा जितना उसकी सरकारें और उसके समर्थक समूह दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। हाँ, भाजपा के सत्ता (1998–2004 और 2014 से अब तक) में आने से पहले ही, अन्य सरकारें, किसी न किसी हद तक, इज़राइल के साथ गहरे संबंधों की खातिर फ़िलिस्तीनी हितों का सौदा करने के लिए तैयार थीं। और हाँ, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों ने भारत और इज़राइल के बीच संबंधों को काफ़ी तेज़ किया है क्योंकि भाजपा, उसके कैडर-आधारित पितृ संगठन, आरएसएस (राष्ट्रीय सेवक संघ) और उसके कई सहयोगी संगठनों के मूल में निहित हिंदुत्व ने हमेशा ज़ायोनवाद के साथ एक ख़ास वैचारिक समानता महसूस किया है।1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा जून 2024 में लगातार तीसरी बार पाँच वर्षीय कार्यकाल के लिए सत्ता में चुनी गई।
यह स्पष्ट रूपरेखा भारत में सरकारी बदलावों की ऐतिहासिक दिशा को दर्शाती है, और यहाँ हम जो मुख्य विवरण प्रस्तुत करेंगे, वह इन केंद्रीय शासकीय परिवर्तनों के समानांतर भारत-इज़राइल-फ़िलिस्तीन संबंधों के विकास को रेखांकित करेगा। भारत के चार अन्य पड़ोसियों—श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश—के साथ इज़रायल के संबंधों की प्रकृति का भी संक्षेप में परीक्षण किया जाएगा।
गांधी और नेहरू
प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के बाद, गांधी और नेहरू जैसे नेताओं का दूसरे जगह हो रहे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्षों से भी जुड़ाव रहता था। 1936 का महान विद्रोह, जो 1939 तक चला2, के बाद फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध के लिए समर्थन स्वाभाविक रूप से बढ़ा। इसके अलावा, गांधी ने अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभावी रूप से सामना करने के सिलसिले में हिंदू-मुस्लिम एकता के निर्माण को अपने दृष्टिकोण की कुंजी माना था। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे अग्रणी मुस्लिम संगठनों का साथ दिया था। लेकिन यहूदी राष्ट्रवाद के उदय और फ़िलिस्तीन में यहूदी बहुसंख्यक राज्य स्थापित करने की ज़ायोनीवादी महत्वाकांक्षा के बारे में क्या हो रहा था? इसके कई प्रमुख पैरोकारों ने इस लक्ष्य के लिए गांधी का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। गाँधी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास (1893-1914) के दौरान हरमन कैलेनबाख और हेनरी पोलाक जैसे कई यहूदियों के साथ उनके घनिष्ठ राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंध थे, जो आगे चलकर ज़ायोनी उद्देश्य के प्रभाव में चले गए। नतीजतन वे गांधी को साथ लाने के लिए अनौपचारिक दूत बन गए।
1931 में गांधी लंदन में भारत में संभावित राजनीतिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने ज्यूइश क्रॉनिकल साप्ताहिक को एक साक्षात्कार दिया। उस साक्षात्कार में उन्होंने ज़ायोनवाद या ‘ज़ायोन की ओर वापसी’ को आंतरिक आध्यात्मिक संतोष की तलाश के रूप में बताया, जो कहीं भी हो सकता है, और वह ‘फ़िलिस्तीन पर फिर से कब्जा करने’ के भौगोलिक दावे से अलग है, जहाँ प्रवास के लिए अरबों की स्वीकृति आवश्यक है। हालाँकि, 1937 के मध्य में कैलनबाख बॉम्बे (अब मुंबई) के बाहर एक आश्रम में गांधी से मिले और वहाँ एक महीने से अधिक समय तक रहकर उन्होंने गांधी को राज़ी कर लिया कि ज़ायोनी आध्यात्मिक संतुष्टि को फ़िलिस्तीन में बसने से अलग नहीं किया जा सकता। इस घटना ने गांधी की सोच में दुविधा पैदा कर दी, जो बाद तक बनी रही, भले ही उन्होंने फिर दोहराया कि बैलफ़ोर घोषणा इसको उचित नहीं ठहरा सकती और ऐसा तब ही किया जाए जब ‘अरब राय इसके लिए तैयार हो’ (Imber 2018)।
आज भारत में वामपंथी पार्टियाँ और उनके बुद्धिजीवी, जो दावा करते हैं कि गांधी कभी दुविधा में नहीं थे, हमेशा उनके 26 नवम्बर 1938 के हरिजन अखबार में लिखे संपादकीय को उद्धृत करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन अरबों का उतना ही है जितना इंग्लैंड अंग्रेज़ों का और फ़्रांस फ़्रांसीसियों का। हाल तक भारत-इज़रायल-फ़िलिस्तीन संबंधों की ऐतिहासिक दिशा पर टिप्पणी और लेखन करने वाले अधिकांश बौद्धिकों का यही प्रमुख और मूलतः निर्विवाद दृष्टिकोण रहा है। भाजपा के सत्ता में आने के साथ, उससे जुड़े कुछ बुद्धिजीवी ‘राष्ट्रपिता’ की विरासत का पुनःव्याख्यान करना चाहते हैं ताकि आज की प्रबल इज़रायल-परस्त नीति को अधिक विश्वसनीयता दी जा सके (Kumaraswamy 2010)।
मार्च 1946 में गांधी ने विश्व यहूदी कांग्रेस के सदस्य मिस्टर हॉनिक और ब्रिटेन की लेबर पार्टी के यहूदी सांसद एस. सिल्वरमैन से मुलाक़ात की। इस चर्चा में गांधी से एक प्रश्न पूछा गया और उनके निजी सचिव प्यारे लाल नैयर द्वारा विधिवत दर्ज किया गया—‘क्या हम यह मान लें कि आप यहूदियों के लिए राष्ट्रीय आवासीय स्थल स्थापित करने की हमारी आकांक्षा से सहानुभूति रखते हैं?’ गांधी का उत्तर दर्ज नहीं किया गया। वास्तव में 1948 में गांधी की मृत्यु के बाद प्यारे लाल ने फ़िलिस्तीन पर कुछ काग़ज़ात चुनिंदा रूप से नष्ट कर दिए। लेकिन सिल्वरमैन ने बाद में अमेरिकी पत्रकार लुई फ़िशर को यह उत्तर बताया, जिन्होंने इस चर्चा के लगभग तीन महीने बाद गांधी से संपर्क किया और इस उत्तर की सत्यता की पुष्टि की। गांधी ने कहा था, ‘मैंने सिल्वरमैन से कहा कि फ़िलिस्तीन में यहूदियों का मामला मज़बूत है। यदि अरबों का दावा है, तो यहूदियों का उनसे पहले का दावा भी है।’ बाद में हरिजन के 21 जुलाई के अंक में गांधी ने कहा, ‘यह सच है कि मैंने इस विषय पर श्री लुई फ़िशर के साथ लंबी बातचीत के दौरान कुछ ऐसा ही कहा था।’ फिर उन्होंने ज़ायोनिस्टों के बारे में कहा कि उन्हें आतंकवाद छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए। ‘वे फ़िलिस्तीन में ज़बरन पैठ बनाने के लिए आतंकवाद का सहारा क्यों लें? यदि वे अहिंसा के बेजोड़ हथियार को अपनाएँ... तो उनका मामला दुनिया का मामला होगा... यह सबसे अच्छा और सबसे उज्ज्वल होगा।’ फिर भी गांधी की समग्र स्थिति का सबसे संतुलित आकलन यह है कि वे फ़िलिस्तीन को अरब नियंत्रण के तहत एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य बनने का समर्थन करते थे। साथ ही वहाँ जाने की यहूदी इच्छा को स्वाभाविक मानते थे और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की बात करते थे। बाद में क्या वे निरंतर यहूदी प्रवास का विरोध किया या नहीं यह ज्ञात नहीं है, लेकिन यह संभव है कि वे यह शर्त जोड़ते कि किसी भी प्रवास पर अरबों की सहमति हो।
नेहरू भी गांधी की तरह ही द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले और उसके दौरान यहूदियों के साथ हुए व्यवहार को देखते हुए उनके प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। लेकिन उनकी यह सहानुभूति, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ मिलकर ज़ायोनी राज्य की स्थापना के प्रयासों का समर्थन करने तक नहीं पहुँची। मई 1947 में फ़िलिस्तीन के सवाल पर गठित संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति (UNSCOP) के 11 सदस्यों में भारत भी शामिल था और इसने ब्रिटेन द्वारा ज़िम्मेदारी सौंपे जाने पर महासभा को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। तब भारत (ईरान और यूगोस्लाविया के साथ) ने संघीय एकता बनाए रखने की योजना पेश की थी। इतना ही नहीं, उसने बहुमत की उस योजना के विरुद्ध मतदान भी किया था, जिसमें फ़िलिस्तीन का विभाजन प्रस्तावित था। इससे यहूदियों को (जो तब लगभग 30% आबादी थे) 55% क्षेत्र मिल जाता, लेकिन अधिकतर बोझ फ़िलिस्तीनियों पर आता। वैसे भी यह योजना केवल सिफ़ारिश थी और उसे थोपा नहीं जाना था। इसके अलावा, फ़िलिस्तीनी पक्ष ने इसे अस्वीकार किया था, क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता देने की प्रतिबद्धता का उल्लंघन करती थी। फिर भी, 1950 में नेहरू ने इज़राइल को मान्यता दे दी, जबकि विभाजन-योजना के विपरीत उसने तब ज़बरन 78% क्षेत्र पर क़ब्ज़ा कर लिया था। सितंबर 1950 में ज्यूइश एजेंसी ने बॉम्बे (अब मुंबई) में एक आव्रजन कार्यालय भी खोला, क्योंकि लगभग 60,000 (बेने और बगदादी) यहूदी भारत में आकर प्रवास कर रहे थे या 18वीं–19वीं शताब्दियों में यहूदी धर्म अपना लिया था।3 यह कार्यालय बाद में व्यापार कार्यालय में और फिर 1953 में एक छोटे वाणिज्य दूतावास में बदल गया।
पहला, 1947–49 के नक़बे के बाद ऐसी कोई वास्तविक स्वतंत्र और प्रतिनिधि राजनीतिक इकाई नहीं थी जो वास्तव में फ़िलिस्तीनी हितों को प्राथमिकता देता। दूसरा, विभाजन के बाद भारत ने पाकिस्तान को मान्यता दी थी, तो इज़रायल को क्यों नहीं? ईरान और तुर्की जैसे दो मुस्लिम बहुल देशों ने पहले ही इज़रायल को मान्यता दे दी थी। इसके अलावा, मई 1949 में इज़रायल को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य स्वीकार कर लिया गया और प्रवेश की शर्त के रूप में उसने विस्थापित फ़िलिस्तीनियों के ‘वापसी के अधिकार’ पर प्रस्ताव 194 को स्वीकार किया, जिसे उसने कभी लागू नहीं किया। तीसरा, सोवियत संघ मई 1948 में इज़रायल को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश था, इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई), जो तब मुख्य विपक्षी शक्ति थी, ने नेहरू का विरोध नहीं किया। आंशिक रूप से अरब भावनाओं का ध्यान रखते हुए, उन्होंने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने से परहेज़ किया। यह व्यावहारिक यथार्थवाद था जिसने पहले नेहरू को मान्यता देने के लिए प्रेरित किया और फिर उन्हें पीछे रोके रखा।
1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध छिड़ गया और जहाँ नेहरू का भारत गुटनिरपेक्ष रवैया अपनाकर अमेरिका-सोवियत प्रतिद्वंद्विता से अलग रहने की कोशिश कर रहा था, वहीं पाकिस्तान अमेरिकी राजनीतिक-सैन्य प्रस्तावों के प्रति अधिक खुला था। इज़रायल के साथ संबंधों को अनिश्चित बनाए रखना, मुस्लिम समर्थन को परेशान नहीं करेगा, लेकिन नेहरू के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य 1952 में गमाल अब्देल नासिर का मिस्र जैसे प्रमुख मध्य-पूर्व देश में सत्ता में आना था। नासिर अरब राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे, उनका नेहरू की ही तरह गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने की ओर झुकाव था और पाकिस्तान से अधिक भारत के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसके अलावा, व्यापार और कूटनीतिक समर्थन के लिए अरब सरकारों के साथ भारतीय संबंध सुधारना नवजात इज़रायल के साथ संबंध तेज़ करने से अधिक लाभकारी माना जा रहा था। दूसरी ओर, उस समय नेहरू चाहते थे ki 1955 के बानदुंग सम्मेलन में, जो बाद में गुटनिरपेक्ष देशों के समूह के गठन का कारण बना, इज़राइल को शामिल कर लिया जाये — यह इस तथ्य को व्यक्त करता है कि फिलिस्तीनी पीड़ाओं का विदेश नीति की सोच पर बहुत कम या कोई असर नहीं था। वास्तव में, दिसम्बर 1954 में इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बर्मा और सीलोन के नेताओं ने बोगोर (जावा) में सम्मेलन की तैयारी के लिए मुलाक़ात की। नेहरू ने बानदुंग में इज़रायल को शामिल करने पर ज़ोर दिया। सौभाग्य से, पाकिस्तान ने इज़रायल से संघर्षरत अरब देशों की भावनाओं की चिंता करते हुए इसे रोक दिया (Anderson 2024)।
1955 में बग़दाद संधि में शामिल होने के साथ पाकिस्तान औपचारिक रूप से अमेरिका के साथ सैन्य रूप से जुड़ गया। इस संधि में ईरान, इराक, तुर्की और ब्रिटेन भी शामिल थे (बाद में इसका नाम सेंटो या सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन रखा गया)। इसका विरोध मिस्र और भारत दोनों ने किया, जिन्होंने उसी वर्ष अपनी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए। 1956 में इजरायल, यूके, फ्रांस द्वारा शुरू किए गए स्वेज आक्रमण और युद्ध के बाद, भारत के इजरायल के साथ गहरे संबंधों की ओर बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। यह राजनयिक ठहराव नेहरू के शासन के आगे 1964–84 की पूरी अवधि तक चला, जिसमें 1967 और 1973 के इज़रायल-अरब युद्ध और 1982 में लेबनान पर इज़रायल का आक्रमण भी शामिल है। हालाँकि, इस राजनयिक ठहराव के बावजूद भारत और इज़रायल के बीच पर्दे के पीछे उल्लेखनीय संपर्क बने रहे। मई 1964 में नेहरू का निधन हो गया, लेकिन 1962 के चीन युद्ध के दौरान भारत को इज़रायल से भारी तोप (मोर्टर) और गोला-बारूद मिला और 1965 तथा 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों में उससे और हथियार ख़रीदे (Bhattacherjee 2017; Essa 2022)।
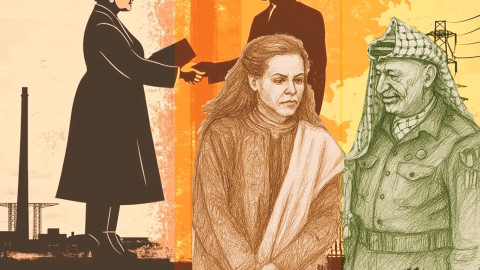
Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
1965 से 1998 तक
1966 में कांग्रेस पार्टी के अंतरिम नेता लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद (जिन्होंने 1965 के युद्ध को समाप्त करते हुए पाकिस्तान के साथ शांति संधि की थी), नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनीं। 1968 में, उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) नामक गुप्त सेवा एजेंसी की स्थापना की और मोसाद के साथ सहयोग करना शुरू किया - उस समय नई दिल्ली और तेल अवीव पाकिस्तान और चीन को साझा दुश्मन मानते थे और श्रीमती गांधी दोनों के बीच, और बाद में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य संबंधों को लेकर चिंतित थीं।
जहाँ तक इज़राइल का सवाल है, ऐसा माना जाता था कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लीबियाई और ईरानी लोगों को चीनी और उत्तर कोरियाई सैन्य उपकरणों को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दे रहे थे (RAW और मोसाद 2003)। इसे गुप्त रखा गया, जबकि 1974 में भारत ने सार्वजनिक रूप से PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी। 1975 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 3379 का सह-प्रायोजन किया, जिसने ज़ायोनवाद को नस्लवाद के बराबर बताया।5 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया और मार्च 1977 में जाकर आम चुनाव बहाल किया, लेकिन वे चुनाव हार गईं। जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का उनका गुट फिर से केंद्रीय सत्ता में आ गया, और कुछ घटनाक्रमों ने भारत और इज़राइल को करीब लाने में सहायता की। लेकिन 1977-79 का अंतराल, जब जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता में थी, अपने आप में महत्वपूर्ण था।
जनता पार्टी उन विभिन्न दलों और राजनीतिक समूहों का एक ढीला ढाला गठबंधन था जिन्होंने साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई थी। इसका सबसे मजबूत घटक (1980 में जनता पार्टी के पतन के बाद बनी बीजेपी का पूर्वज) हिंदू राष्ट्रवादी जनसंघ था, जो हमेशा से इजराइल का पक्षधर रहा था, क्योंकि वह उसे मध्य-पूर्व के मुस्लिम-बहुल देशों के खिलाफ अहम गढ़ मानता था। इसके मुख्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे और इसी वजह से उस समय भारत में इज़राइल के विदेश मंत्री मोशे दयान की गुप्त यात्राओं का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगस्त 1977 में उन्होंने वाजपेयी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की। हालाँकि भारत की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इस यात्रा का होना ही इस बात का संकेत था कि नयी हवाएँ चलने लगीं हैं, चाहे वह हल्की ही क्यों न हों।
रॉ (RAW) और मोसाद का सहयोग पहले से ही शुरू हो चुका था, और निस्संदेह दयान की यात्रा की व्यवस्था में इसका योगदान रहा था। कहा जाता है कि 1978 में वे फिर आए और शायद नेपाल में भारत के वरिष्ठ समकक्षों तथा संभवतः रॉ के शीर्ष अधिकारियों से मिले।6 ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवधि में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें पाकिस्तान के कहूटा यूरेनियम संवर्द्धन संयंत्र पर संयुक्त हमले का इज़रायली प्रस्ताव भी शामिल था, ताकि परमाणु बम बनाने को रोका जा सके। केवल भविष्य में ही, गुप्त सरकारी कागज़ात के खुलासे से यह पुष्टि या खंडन हो सकेगा कि इन चर्चाओं में दयान की भूमिका थी या नहीं। लेकिन अन्य स्रोत यह स्पष्ट करते हैं कि 1982-84 के बीच किसी समय ऐसे संयुक्त हमले की योजना बनी थी, परंतु अंतिम समय पर इसे रद्द कर दिया गया।7 आखिरकार, 1981 में इज़राइल ने ठीक ऐसा ही किया था जब उसने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर को नष्ट कर दिया था।
1984 में गांधी की हत्या के बाद, कांग्रेस ने चुनावों में भारी जीत हासिल की और उनके पुत्र राजीव गांधी, जिन्होंने पहले अपने परिवार की राजनीतिक विरासत में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, प्रधानमंत्री बने। 1 अक्टूबर 1985 को इज़राइल ने तूनिस में PLO मुख्यालय पर हवाई हमला किया, जिसमें 60 पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए, और जिसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शीघ्र ही निंदा की। उसी महीने बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर न्यूयॉर्क शहर पहुँचे और इस भीषण हमले के बावजूद, उन्होंने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस से निजी मुलाकात करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। यह दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की पहली मुलाकात थी, जो अपने आप में ही फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत की नई संवेदनहीनता को दर्शाती थी।
भारत के रूख में यह बदलाव खुद PLO के दृष्टिकोण के बदलने से और भी आसान हो गया। 1982 के लेबनान पर इज़रायली युद्ध के बाद PLO के नेतृत्व फतह को सुदूर तूनिसीया में खदेड़ दिया गया। इसके अलावा, उसके नेतृत्व को यह और अधिक साफ हो गया कि उसकी गुरिल्ला रणनीति उसे जीत की ओर नहीं ले जा रही है। वास्तव में, 1987 में अधिकृत क्षेत्रों (Occupied Territories) में पहला इंतिफ़ादा स्थानीय नेतृत्त्व में हुआ था। हालांकि देश-निष्कासित फतह ने इंतिफ़ादा के समर्थन मे अवश्य ही भूमिका निभाई, लेकिन विद्रोह का एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व (Unified National Leadership of the Uprising - UNLU) मुख्य रूप से स्थानीय सामुदायिक परिषदों और उनके नेताओं को लेकर बना, साथ में इसमें फ़तह के ही नहीं बल्कि अन्य फ़िलिस्तीनी गुटों, जैसे हमास, इस्लामिक जिहाद, वामपंथी पॉपुलर फ्रंट, डेमोक्रेटिक फ्रंट और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि एंव वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल थे।
इंतिफादा के बाद, अराफात के नेतृत्व में PLO ने दो-राज्य समाधान को स्वीकार करने की दिशा में एक मौलिक रणनीतिक बदलाव किया, जिसमें इजरायल द्वारा कब्जाई गई कुल भूमि के केवल 22% पर दावा किया गया, अर्थात वह हिस्सा जिस पर इजरायल ने 1967 के युद्ध के बाद कब्जा कर लिया था। इससे नई राजनीतिक गतिशीलता पैदा हुई, जो अंततः 1993-95 के ओस्लो समझौते का कारण बनी, जिसका मुख्य परिणाम नव-स्थापित फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के शासक के रूप में फतह का इज़राइली कब्जे को बनाए रखने वाले उप-ठेकेदार के तौर पर उभरना था। कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री नरसिंह राव की सरकार (1991-96) के तहत भारत के लिए 1992 में इज़राइल को पूर्ण मान्यता देने का रास्ता साफ़ हो गया, जिसके तहत दिल्ली और तेल अवीव में दूतावास खोले गए। इसके बाद, नई दिल्ली में आने वाली हर सरकार ने एक ओर तो फ़िलिस्तीनी हितों के लिए दिखावटी वादे किए और यहाँ तक कि धन भी खर्च किया, वहीं दूसरी ओर इज़राइल के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, 'साइबर-सुरक्षा' और 'आतंकवाद-विरोधी' संबंधों को लगातार मज़बूत किया।
अति-दक्षिणपंथ का उदय
जून 1996 में 13 दलों वाली एक ग़ैर-कांग्रेसी और ग़ैर-भाजपाई गठबंधन, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन मार्च 1998 तक गिर गई। इसी दौरान इजरायल को मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), ग्रीन पाइन रडार प्रणाली और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए आपसी समझौते हुए। इसके बाद 1998-99 में पहली बार भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार बनी, जो कि फिर 1999 से 2004 तक पाँच साल के कार्यकाल के लिए चुनी गई, दोनों ही बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित हुईं। 2003 में उनके शासनकाल के दौरान ही एरियल शेरोन के रूप में पहली बार किसी इज़राइली प्रधानमंत्री की भारत में आधिकारिक यात्रा हुई थी। इससे पहले 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में, इज़राइल ने भारत को सैन्य सहायता की थी, जबकि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद पर दबाव डालकर उसकी सेना को पीछे हटने को मजबूर किया था। मई 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों पर अमेरिका का शुरुआती गुस्सा जल्द ही शांत हो गया और भारत-इज़राइल-अमेरिका के बीच एक नया सामरिक गठबंधन बनने लगा। लेकिन बड़ी सफलताएँ लगभग एक दशक बाद मोदी के शासनकाल में मिलीं।
वाजपेयी और मोदी के बीच दस साल का अंतराल (2004-14) रहा, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस-नीत गठबंधन ने लगातार दो चुनाव जीते। यह भूल जाइए कि अतीत में नेहरू और श्रीमती गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में, व्यावहारिक कूटनीतिक दबावों के बावजूद, फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति एक हद तक सच्ची नैतिक और राजनीतिक सहानुभूति और समर्थन था। अब इज़राइल के साथ संबंध मज़बूत हो गए थे, जबकि फ़िलिस्तीनी मुद्दे के प्रति वास्तविक चिंता लगभग ख़त्म हो गई थी। उचित फ़िलिस्तीनी राज्य का उदय नहीं हुआ था, जबकि इज़राइल एक शक्तिशाली और काफ़ी विकसित पूंजीवादी राज्य था, जिससे दोनों ओर के व्यवसायों के लिए लाभकारी आर्थिक रिश्ते बनाए जा सकते थे। इसके अलावा, उच्च-गुणवत्ता वाले सैन्य उपकरणों का स्रोत होने के साथ-साथ, इज़राइल अमेरिका के लिए एक तरह का बिचौलिया भी था। उसके साथ नजदीकी संबंधों ने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और राजनीतिक रूप से घनिष्ठ संबंधों की संभावना को बढ़ाया है। केवल कभी-कभार ‘दो-राज्य समाधान की आवश्यकता’ तथा इसके लिए धन की व्यवस्था के बारे में बयानबाजी ही बची रही।
26 नवंबर, 2008 को मुंबई में पाकिस्तान स्थित दो इस्लामी समूहों द्वारा किए गए आतंकी हमले के बाद, इज़राइल ने भारत में निर्दिष्ट केंद्रीय निगरानी प्रणाली (Central Monitoring System) के तहत एक निगरानी ढांचा तयार करने में मदद की, जिसने लक्षित निगरानी से लेकर जन-व्यापक निगरानी तक की क्षमता विकसित की (एस्सा 2023: 48)। नवंबर 2008 के हमलों के समय और उसके तुरंत बाद, उच्च-स्तरीय राजनीतिक संवादों के अलावा, इज़राइल ने खुफिया अधिकारी, पैरामेडिक्स, रिजर्विस्टों की एक टीम और कुछ स्वयंसेवकों को भेजा, जिन्होंने सलाह, सामग्री सहायता के साथ-साथ इस बात की आलोचना की कि इस तरह के आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए भारत की तैयारियाँ कितनी अपर्याप्त थीं। इस अवसर पर इज़राइली कर्मियों की उपस्थिति ने एक व्यापक आम सहमति गढ़ने में मदद की कि भारत की कुछ गंभीर कमियाँ रही हैं जिनके लिए इज़राइल की विशेष निपुणता की आवश्यकता है। यह कहा गया कि अब गुणात्मक रूप से एक नया और गहरा गठजोड़ बन चुका था (Machold 2024)।
2003 से 2013 के बीच भारत इज़राइल का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बन चुका था। फरवरी 2014 में, जब आम चुनाव कुछ महीनों दूर थे और कांग्रेस अब भी सत्ता में थी, तब एक औपचारिक समझौता हुआ (जिसे मई 2014 में मोदी की चुनावी जीत के बाद लागू किया गया) जिसके तहत भारतीय पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को ‘आतंकवाद-रोधी’, ‘भीड़ नियंत्रण’ और ‘सीमा प्रबंधन’ के प्रशिक्षण के लिए इज़राइल भेजा जाना था। इसका अर्थ यह था कि देश के भीतर खासकर पूर्वोत्तर और कश्मीर जैसे विद्रोहग्रस्त इलाक़ों से निपटने के तौर-तरीके सिखाए जाएँ। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों दोनों को राजनीतिक आत्मनिर्णय का अधिकार नकारते हुए, भारी सैन्य उपस्थिति ने कश्मीर को भी उसी तरह एक स्थायी सैन्य कब्ज़े का क्षेत्र बना दिया जैसा कि फ़लस्तीन के कब्ज़ाए गए क्षेत्रों (Occupied Territories) में है। फ़लस्तीनियों और कश्मीरी मुसलमानों, दोनों के लिए हिंसा एक सामान्य और वैधानिक रूप से जायज़ ठहराई गई प्रक्रिया है, जिसमें सबसे अलोकतांत्रिक और दमनकारी क़ानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर में हिंदुओं के लिए बस्तियाँ बनाने का काम उनकी ज़मीन पर अधिक कब्ज़ा करके किया जा रहा है, और केंद्र सरकार की अलग-अलग परियोजनाओं के लिए भी। हिंदू-मुसलमानों को अलग करने का यह ढाँचा इज़राइल की वेस्ट बैंक नीति से मेल खाता है (Essa 2022)।
2003 और 2013 के बीच, भारत इज़राइल का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बन गया था। फरवरी 2014 में, जब आम चुनाव अभी कुछ महीने दूर थे और कांग्रेस अभी भी सत्ता में थी, तब एक औपचारिक समझौता हुआ (जिसे उस वर्ष मई में मोदी की चुनावी जीत के बाद अमल में लाया गया) कि भारतीय पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को इज़राइल में 'आतंकवाद-निरोध', 'भीड़ नियंत्रण' और 'सीमा प्रबंधन' का प्रशिक्षण दिया जाए, यानी उन्हें अपने देश में, खासकर पूर्वोत्तर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर में, समस्याओं से निपटने के तरीके सिखाए जाएँ। फ़िलिस्तीनियों और कश्मीरियों को 'राजनीतिक आत्मनिर्णय के अधिकार' से वंचित करने के अलावा, सशस्त्र कर्मियों की भारी मौजूदगी, कश्मीर को, जैसा कि फ़िलिस्तीन के अधिकृत क्षेत्रों में होता है, निरंतर सैन्य कब्जे और नियंत्रण का केंद्र बना देती है । आगे, फ़िलिस्तीनियों और कश्मीरी मुसलमानों, दोनों के लिए, हिंसा रोजमर्रा के मामले की तरह है और इसे सबसे अलोकतांत्रिक और दमनकारी कानूनों के इस्तेमाल द्वारा वैधानिक रूप से उचित ठहराया जाता है। कश्मीर के भारतीय हिस्से में हिंदुओं के लिए बस्तियों के निर्माण, केंद्र सरकार के विभिन्न उद्देश्यों और हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु अधिकाधिक भूमि अधिग्रहण मोटे तौर पर वेस्ट बैंक में इजरायल की नीति के समान है (Essa 2022)।8
लेकिन ज़ायोनवाद के प्रति हिन्दुत्व की वैचारिक रिश्तेदारी का भाव, मोदी युग में आकर इजरायल द्वारा अधिकृत क्षेत्रों में फिलिस्तीनी 'शत्रु' के साथ किए गए व्यवहार के प्रति अधिक स्पष्ट प्रशंसा और वास्तव में अनुकरण की भावना में बदल गया।
2014 के मध्य से भारत-इज़राइल संबंधों में आए महत्त्वपूर्ण (और कुछ मामलों में गुणात्मक) बदलाव पर ध्यान देने से पहले, हमें भारत के चार दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और उनके ऐतिहासिक व समकालीन इज़राइल-संबंधों पर ध्यान देना होगा। यह कई कारणों से ज़रूरी है। भारत-पाकिस्तान-इज़राइल संबंधों का राजनीतिक महत्व स्पष्ट है। हिंदुत्ववादी भारत के लिए इज़राइल उसका अहम सहयोगी है, जो उसके प्राथमिक शत्रु पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ा है। बांग्लादेश दिसंबर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना। तब से बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, भारत की उप-साम्राज्यवादी क्षेत्रीय प्रभुत्व की महत्वाकांक्षा से अधिक भयभीत रहते हैं और उनकी विदेश नीति का रुख़ उसी के अनुरूप ढलता है। बांग्लादेश के मामले में, उसका मुस्लिम तत्व इजरायल के प्रति उसके कूटनीतिक-राजनीतिक विरोध तथा राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर भारत और इजरायल के बीच बढ़ते गठजोड़ से उसकी बेचैनी को स्पष्ट करता है। श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे और कमज़ोर राष्ट्र फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति शुरू से ही उदासीन रहे हैं और शुरुआती भारत के विपरीत, उन्हें इज़राइल से बेहतर संबंध बनाने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं रही। हालांकि श्रीलंका में कभी-कभार घरेलू वामपंथी दबावों के चलते उलट-पलट होता रहा। नेपाल में आंतरिक वामपंथी ताक़तों के साथ समझौते नई सहस्राब्दी में ही सामने आए और उन्हें जल्दी ही काबू कर लिया गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल चीन के साथ मज़बूत रिश्तों को भारत के लिए एक संतुलनकारी ताक़त मानते हैं, और बाद के दो (श्रीलंका व नेपाल) निहायत राजनीतिक-राजनयिक कारणों से यह नहीं चाहते कि भारत का इज़राइल से संबंधों पर एकाधिकार हो।
श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश
श्रीलंका
श्रीलंका (जिसे 1972 तक सीलोन कहा जाता था) ने 4 फरवरी 1948 को औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी पहली सरकार यूनाइटेड नेशनल पार्टी (UNP) की थी और प्रधानमंत्री बने डी. एस. सेनानायके। वस्तुतः यह पहला एशियाई देश था जिसने इज़राइल से संबंध स्थापित किए। 1950 के दशक की शुरुआत में उसने इज़राइल से हथियार और यहाँ तक कि एक युद्धपोत भी खरीदा। यह श्रीलंका फ़्रीडम पार्टी (SLFP) को पसंद नहीं आया, जो अधिक वामपक्षीय सामाजिक जनतांत्रिक रूप की विपक्षी पार्टी थी और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति चाहती थी। इसने पहली बार 1956 में एस. डब्ल्यू. आर. डी. बंडारनायके के नेतृत्व में और फिर 1960-64 में उनकी पत्नी सिरिमावो बंडारनायके (दुनिया की पहली निर्वाचित महिला प्रधानमंत्री) के नेतृत्व में चुनावी जीत हासिल की। सिरिमावो और SLFP, PLO के साथ रिश्ते मज़बूत करने के इच्छुक थे और अपनी ही पार्टी से भी अधिक वामपंथी दलों और समूहों के दबाव का सामना करती हुईं, 1971 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इज़रायली दूतावास बंद करने का वादा किया और जीतने के बाद उन्होंने ऐसा ही किया।
सत्तर के दशक के मध्य और अंत तक तमिल आबादी के ख़िलाफ़ भेदभाव के चलते उनके विरोध में वृद्धि हुई, विशेषकर देश के उत्तरी जाफ़ना क्षेत्र में। इसी दौरान एक अधिक उग्र संगठन, ‘लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम’ (LTTE) उभरा। 1977 में UNP फिर सत्ता में लौटी और इसके नेता जे. आर. जयवर्धने प्रधानमंत्री बने और फिर संविधान संशोधन के बाद 1978-89 तक शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति रहे। उन्होंने इज़राइल से संबंध बहाल किए, मुख्य कारण सैन्य सहयोग पाना था। भारत (राजीव गांधी के नेतृत्व में) इज़राइल से बेहतर संबंध चाहता था लेकिन दक्षिण एशिया को भारत का प्रभावक्षेत्र मानता था। इज़रायली सैन्य सहयोग को 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के ज़रिए प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें पहली बार भारत ने अपने सैनिकों को किसी दूसरे देश भेजकर वहाँ की गृहयुद्ध परिस्थिति में हस्तक्षेप किया। यह LTTE से लड़ने के लिए था, जिसे पहले नई दिल्ली ने, अपने दक्षिण भारत के तमिलों की भावनाओं को देखते हुए, समर्थन दिया था। LTTE को कमज़ोर करने में असफल रहने पर, नए श्रीलंकाई राष्ट्रपति आर. प्रेमदासा (1989-93) ने गांधी से सभी सैनिक वापस बुलाने को कहा और मार्च 1990 तक भारत ने अपने सैनिक हटा लिए (Amarasinghe 2021; 2023)।
फिर भी, इज़राइल को लेकर श्रीलंका की नीतियाँ अस्थिर बनी रहीं। श्रीलंका की लगभग 10% आबादी मुसलमान है, जो ज़्यादातर उत्तर-पूर्व में बसती है। उनका समर्थन पाने और उन्हें LTTE से अलग करने के लिए—जिसे अंततः 2009 में सैन्य रूप से हराया गया—प्रेमदासा ने 1992 में इज़राइल से संबंध तोड़ दिए। लेकिन 2000 में इसे फिर से बहाल किया गया क्योंकि श्रीलंका फिर से सैन्य सहयोग चाहता था और इज़राइल पश्चिमी हथियार प्रतिबंधों की अवहेलना करने को तैयार था। तब से द्विपक्षीय संबंधों में कोई गंभीर व्यवधान नहीं आया। 7 अक्टूबर 2023 के बाद श्रीलंका ने इज़राइल की मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और वहाँ से निकाले गए फिलिस्तीनियों की जगह अपने मज़दूर भेजने की अनुमति दी। हाल के वर्षों में श्रीलंका के घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल ने अंततः एक लोकप्रिय विद्रोह को जन्म दिया, जिसने पूर्ववर्ती सरकार को उखाड़ फेंका और ‘नेशनल पीपल्स पावर’ (NPP) नामक कथित तौर पर वामपंथी पार्टी को सत्ता में लाया, जिसने नवंबर 2024 में संसदीय चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया और एक नए राष्ट्रपति ए. के. डिसानायके (जिनका वामपंथी अतीत है) को सत्ता सौंपी। यह नई सरकार ग़ज़ा में युद्धविराम और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय की मांग में अधिक मुखर है। हालांकि, इज़राइल के लिए मज़दूर भेजने की प्रक्रिया अब भी जारी है और हाल में विशेष क्षेत्रों में कामगार भेजने के समझौते हुए हैं, जिन्हें कोलंबो ने यह कहकर सही ठहराया है कि यह लाभकारी है और अन्य देश भी इज़राइल के साथ आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं (Balachandran 2023)।
पाकिस्तान
पाकिस्तान उन देशों में से है जिन्होंने आज तक इज़राइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं स्थापित किए हैं। आधिकारिक तौर पर उसे इज़राइल के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन तीसरे देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के माध्यम से एक परोक्ष मार्ग मौजूद है। फिर भी यह बहुत सीमित है और अधिकांशतः इसमें इज़राइल को कपड़ों का निर्यात शामिल है, जिसका 2023 में अनुमानित मूल्य 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022 में पाकिस्तान ने मुख्यतः केवल 39,000 अमेरिकी डॉलर मूल्य का चिकित्सीय उपकरण आयात किया।9 इसकी तुलना इज़राइल और सऊदी अरब या UAE के बीच परोक्ष व्यापार स्तर से करें तो अब, अब्राहम समझौतों के बाद, यह अधिक प्रत्यक्ष है और वर्तमान में सालाना कई अरब डॉलर तक पहुँच रहा है। इस्लामाबाद में सभी सरकारें फिलिस्तीन को अपने औपचारिक और भौतिक समर्थन निरंतर देती रही हैं। 1967 और 1973 के युद्धों में पाकिस्तानी लड़ाकू पायलटों ने जॉर्डन और इराक की तरफ से फिलिस्तीन की मदद के लिए लड़ाई लड़ी और 1982 के इज़राइल-लेबनान युद्ध के दौरान देश ने PLO की तरफ से लड़ने के लिए स्वयंसेवक भेजे।
पाकिस्तान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन लगभग लगातार रहा है और, भारत के विपरीत, ऐसा न करने के लिए कोई आंतरिक दबाव नहीं है। उसने बार-बार घोषणा की है कि केवल एक ‘व्यवहार्य’, ‘स्वतंत्र’ और ‘सन्निहित’ फिलिस्तीनी राज्य के उदय के बाद ही वह इज़राइल के साथ घनिष्ठ संबंधों की ओर बढ़ने पर विचार करेगा। उसने ओस्लो समझौतों का सावधानीपूर्वक स्वागत किया और अब्राहम समझौतों के समर्थन से खुद को दूर रखा, यह दोहराते हुए कि इज़राइल की ओर किसी भी पहल से पहले दो-राज्य समाधान के पक्ष में उसका अपना रुख अपरिवर्तित बना हुआ है।
हालाँकि, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीनी हित सर्वोपरि हैं और वे सरकार की सोच और व्यवहार को आकार देते हैं, या फिर सरकारी निर्णयकर्ताओं को व्यावहारिक कूटनीतिक चिंताएँ नहीं हैं। अफ़ग़ानिस्तान पर सोवियत कब्ज़े (1979-89) के दौरान अमेरिका द्वारा आयोजित ‘ऑपरेशन साइक्लोन’ के तहत धन और हथियार, जिसमें इज़राइल का भी योगदान था, काबुल और मास्को के विरुद्ध मुजाहिदीन प्रतिरोध को मदद देने के लिए पाकिस्तान में पहुँचाए गए। लेकिन इसका इज़राइल के साथ संबंधों में किसी भी गर्मजोशी से कम, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों से ज़्यादा लेना-देना था। निश्चित रूप से, तेल अवीव इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंध खोलना चाहेगा। नेतन्याहू ने 2018 में भारत यात्रा के दौरान कहा भी था कि उनका देश खुद को पाकिस्तान का शत्रु नहीं मानता और पाकिस्तान को इज़राइल के प्रति शत्रु की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।
हालाँकि, तीन कारण हैं जो आने वाले कुछ समय तक इस्लामाबाद के रुख में किसी भी बदलाव का अनुमान लगाना मुश्किल बनाते हैं। पहले उल्लेख किया गया है कि 1980 के दशक की शुरुआत में भारत और इज़राइल के बीच कहूटा पर बमबारी करने की योजना बनी थी और बाद में पाकिस्तान की निराशा जब अमेरिका और इज़राइल के भारत से संबंध कहीं अधिक मजबूत हो गए। भारत के विपरीत, वहाँ घरेलू स्तर पर फिलिस्तीन के समर्थन में कहीं अधिक ताकत है—सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक इस्लामी समूहों से ही नहीं बल्कि आम जनता से भी। यह सरकार की चाल-चलन की गुंजाइश को सीमित करता है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद समय-समय पर अपने लाभ के लिए फिलिस्तीनियों पर इज़राइल के क्रूर कब्ज़े की तुलना भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत पर कब्ज़े से करता है। फिर इज़राइल जो कर रहा है उस पर आलोचना को नरम करना, विशेषकर ग़ाज़ा पर उसके वर्तमान चल रहे जनसंहारक हमले के बाद, उस मानवीय तर्क को कमज़ोर कर देगा जो वह भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ पेश करने की कोशिश करता है। अंततः, कई मुस्लिम-बहुल देश जिनसे पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हैं जैसे तुर्की और ईरान, किसी भी ऐसे बदलाव से काफ़ी विचलित होंगे।
हालाँकि, तीन कारण इस्लामाबाद के रुख में आने वाले कुछ समय तक किसी भी बदलाव का अनुमान लगाना मुश्किल बनाते देते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में भारत और इज़राइल के बीच कहुटा पर बमबारी की योजना का ज़िक्र पहले भी किया जा चुका है, और उसके बाद पाकिस्तान को निराशा हुई जब अमेरिका और इज़राइल दोनों के संबंध भारत के साथ काफ़ी मज़बूत हो गए। भारत के विपरीत, घरेलू स्तर पर फिलिस्तीन के लिए न केवल धार्मिक और राजनीतिक इस्लामी समूहों का, बल्कि आम जनता का भी काफ़ी समर्थन है। इससे सरकारी दाँवपेंच का दायरा सीमित हो जाता है। यहाँ तक कि इस्लामाबाद भी अपने फ़ायदे के लिए, समय-समय पर इज़राइल के फिलिस्तीनियों पर क्रूर कब्ज़े की तुलना जम्मू-कश्मीर प्रांत पर भारत के कब्ज़े से करता है। ऐसे में इज़राइल की आलोचना को कमज़ोर करना, खासकर गाज़ा पर उसके वर्तमान नरसंहारी हमले के बाद, भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ उसके द्वारा बनाए गए मानवीय तर्क को कमज़ोर कर देगा। अंततः, तुर्की और ईरान जैसे कई मुस्लिम बहुल देश, जिनके साथ पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध हैं, ऐसे किसी भी बदलाव से काफ़ी विचलित होंगे।
बांग्लादेश और नेपाल
बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ और इज़राइल ने उसे तुरंत मान्यता दे दी। लेकिन बांग्लादेश ने पारस्परिकता नहीं दिखाई और दो राज्य समाधान की वकालत करते हुए फ़िलिस्तीनी दूतावास की मेजबानी की। वह अन्य मुस्लिम बहुल देशों की तरह, तीसरे देशों की बढ़ती संख्या के माध्यम से — एशिया के देशों, मध्य पूर्व और हाल ही में यूरोप और अमेरिका के माध्यम से इज़राइल के साथ अप्रत्यक्ष व्यापार करता है। बांग्लादेश का इज़राइल के साथ पर्याप्त व्यापार अधिशेष (trade surplus) है — 2023 में इज़राइल को इसके निर्यात (मुख्य रूप से वस्त्र, जूते और चमड़े के सामान) 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गए थे, जबकि प्लास्टिक और चिकित्सीय उपकरणों का उसका आयात 2022 में 148,000 अमेरिकी डॉलर तक गया। हालाँकि, इसमें यह तथ्य शामिल नहीं है कि इस संदेह के उचित आधार हैं कि बांग्लादेश ने इज़राइल से निगरानी उपकरण खरीदे हैं और साथ ही हंगरी और थाईलैंड जैसे तीसरे देशों में इज़राइली बलों से उसके सुरक्षाकर्मियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।10 जनांदोलन के परिणामस्वरूप, अगस्त 2024 में पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार गिर गई (वह भारत भाग गईं), संसद भंग कर दी गई और पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार सत्ता में आई, जिसने चुनावी प्रणाली में सुधार और लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए संवैधानिक बदलावों का वादा किया। इज़राइल के साथ द्विपक्षीय संबंधों के पिछले स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया है।
दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का इज़राइल के साथ सबसे मैत्रीपूर्ण और कम तनावपूर्ण संबंध रहा है। ब्रिटेन ने 1923 में उसे एक स्वतंत्र राजशाही के रूप में मान्यता दी। 1951 के लोकतांत्रिक आंदोलन के परिणामस्वरूप अंततः 1959 में पहले आम चुनाव हुए और नेपाली कांग्रेस के नेता, प्रधानमंत्री बी.पी. कोइराला ने पहली बार इज़राइल का दौरा किया। अगले वर्ष, नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश बना जिसने इज़राइल को पूर्ण राजनयिक मान्यता प्रदान की। इज़राइल ने 1961 में काठमांडू में अपना दूतावास स्थापित किया, हालाँकि नेपाल ने बहुत बाद में ऐसा किया। तब से, यहाँ तक कि 2008 और 2012 के बीच जब माओवादी सत्ता में थे, तब भी द्विपक्षीय संबंध निरंतर रहे हैं। निस्संदेह, नेपाल मध्य पूर्व में शांति और इज़राइल तथा फ़िलिस्तीन दोनों के साथ-साथ रहने वाले द्वि-राज्य समाधान के सामान्य आह्वान को कर्तव्यनिष्ठा से दोहराता है और क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने वाले सभी उपायों के लिए अपना समर्थन व्यक्त करता है। लेकिन इस दौरान वह PLO के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने से बचता रहा है।
अपने पड़ोसियों के विपरीत, नेपाल ने 1975 के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें ज़ायोनवाद को नस्लवाद के बराबर बताया गया था। इज़राइल का नेपाल के साथ आर्थिक सहयोग नियमित रहा है, जिसमें उसके द्वारा प्रदान किया गया कुछ सैन्य प्रशिक्षण भी शामिल है। बढ़ते इज़राइली पर्यटन से नेपाल को अपने व्यापक द्विपक्षीय व्यापार घाटे की आंशिक रूप से भरपाई करने में मदद मिलती है। नेपाल मुख्यतः ऊनी कपड़े, तंबाकू, जूट और सब्जी उत्पादों का निर्यात करता है और कृषि उपकरण तथा इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जैसी वस्तुओं का आयात करता है। इज़राइल में नेपाली महिला सहायक कर्मियों (caregivers) का स्वागत किया जाता है, लेकिन अधिकांश प्रवासी धन अरब मध्य पूर्व में काम करने वाले नेपालियों से आता है। यही कारण है कि काठमांडू कई बार इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ प्रस्तावों पर बहुमत के साथ हो कर मतदान करता है जिससे तेल अवीव को थोड़ी परेशानी होती है।
नेपाल सरकार ने 7 अक्टूबर 2023 की हमास कार्रवाई की कड़ी निंदा की, जब किबुत्ज़ अलुमिम में 10 नेपाली कृषि छात्र मारे गए। लेकिन भारत की ही तरह, नेपाल ने गाजा पर इजरायल के हमले का वर्णन करने के लिए नरसंहार या नरसंहारक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और न ही उसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के हस्तक्षेप के लिए दक्षिण अफ्रीका का समर्थन किया। जब अक्टूबर 2024 में इजरायल ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के शांति सेना पर हमला किया, तो अन्य 33 देशों के साथ, जिनके सैनिक UNIFIL में शामिल हैं, नेपाल ने संयुक्त बयान जारी किया, जो दक्षिण लेबनान में हमले की निंदा तो करता है परंतु इजरायल का नाम लेकर उस पर आरोप लगाने से बचता है। मई 2025 में, गाजा में इजरायल जो कुछ भी कर रहा है उसके बावजूद, इजरायल और नेपाल के बीच निरंतर राजनयिक और भौतिक समर्थन और सहयोग के औपचारिक राजनयिक आश्वासन दिए गए थे।

Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
मोदी युग
जून 2014 में सत्ता में आने के बाद, मोदी ने जल्दी दिखा दिया कि वे इज़राइल को अलग ढंग से देखेंगे। इसके विरोधाभास पर ध्यान दें: 31 मई 2010 को, इज़राइल ने तुर्की से ग़ाज़ा जा रही छह जहाज़ों की राहत बेड़े (फ्लोटिला) पर हमला किया। पंद्रह अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ता मारे गए और कई घायल हुए। उस समय कांग्रेस-नेतृत्व वाली सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की, लेकिन सीधे इज़राइल का नाम नहीं लिया। जुलाई 2014 में कथित तौर पर हमास ने रॉकेटों से बदले की करवाई किया जिसमें इज़राइल के एक सैनिक और छह नागरिकों की मौत हो गई। इज़राइल ने ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज शुरू किया जो 50 दिनों तक ज़मीनी और हवाई आक्रमण के रूप में चला, जिसने ग़ाज़ा के बड़े हिस्से को ध्वस्त कर दिया। इसमें 2,251 फ़िलिस्तीनी मारे गए (घायल होने वालों की गिनती नहीं), जिनमें 1,462 नागरिक थे। कुछ दिनों बाद विपक्ष ने लोकसभा में इज़राइल की निंदा का प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की, लेकिन मोदी ने इस प्रस्ताव को रोक दिया। जहाँ पहले भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के इसराइल की निंदा करने वाले प्रस्तावों का समर्थन करता था, अब वह अधिकतर बार इस तरह के प्रस्तावों में वोटिंग से बाहर रहने लगा।
2017 में इज़राइल की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। तीन दिनों की इस यात्रा में दोनों देशों के संबंधों को औपचारिक रूप से ‘रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया गया। उन्होंने फ़िलिस्तीनी नेतृत्व से मुलाक़ात नहीं करके उस परंपरा को भी तोड़ा जिसमें भारतीय नेता हमेशा फ़िलिस्तीनी नेतृत्व से मुलाक़ात करते थे। जानबूझकर संदेश देने की कोशिश की गई कि फ़िलिस्तीनी प्रश्न अब अप्रासंगिक हो गया है और अब भारत-इज़राइल संबंधों का सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इसी समय मोदी सरकार ने पेगासस खरीद के लिए एक समझौता किया था। यह एक सैन्य स्तर का स्पाइवेयर को एक इज़राइली फर्म द्वारा केवल सरकारों को बेचा जाता है।
2018 में टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटिज़न लैब ने पाया कि इसका इस्तेमाल भारत सहित 45 देशों में मैलवेयर इंस्टॉल करने और निगरानी करने के लिए किया जा रहा था। 2021 में इसका इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मोदी शासन की आलोचना करने वाले पत्रकारों और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सहित कम से कम 300 भारतीयों पर अवैध रूप से किया जा रहा था (शांता 2019)।11 भारत सरकार द्वारा न तो कभी इसको नकारा और न ही इसको स्विकार किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट उत्तर मांगने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
10 फ़रवरी 2018 को मोदी ने रामल्लाह के तीन घंटे के दौरे में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (पीए) के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाक़ात की। वहाँ लंबे समय से चला आ रहा आधिकारिक भारतीय घोषणा-पत्र को दोहराया गया, जिसमें ‘संप्रभु और स्वतंत्र’ फ़िलिस्तीनी राज्य के समर्थन की बात कही गई। लेकिन पहली बार ‘एकीकृत’ फ़िलिस्तीनी राज्य और पूर्वी येरुशलम को उसकी राजधानी बताने का ज़िक्र नहीं किया गया।
निहितार्थ स्पष्ट था, नई दिल्ली भविष्य में किसी बंटुस्तान प्रकार के दो-राज्य समाधान को, जैसा इज़राइल चाहेगा, आराम से स्वीकार कर लेगी। इज़राइली हिंसा, चाहे ग़ाज़ा की नाकेबंदी हो या पश्चिमी तट पर अवैध बस्तियों का विस्तार, भारत इससे न तो नैतिक रूप से परेशान था, न ही राजनीतिक रूप से। 2020 के अब्राहम समझौते का नई दिल्ली ने सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया। 14 जुलाई 2022 को I2U2 (भारत-इज़राइल-यूएई-अमेरिका) समूह स्थापित हुआ ताकि संयुक्त आर्थिक उद्देश्य पूरे किए जा सकें। कुछ ही घंटों बाद हाइफ़ा बंदरगाह अदाणी पोर्ट्स को बेच दिया गया, ताकि इज़राइली कंपनी गाडोर (Gador)12 के साथ मिलकर इसका संचालन किया जा सके। भारत–मध्यपूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन में शुरू हुआ, जब भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ़्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह अभी यह व्यावहारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है, इसका विकास ग़ाज़ा युद्ध के कारण रुका हुआ है।
7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद मोदी सरकार ने निंदा की और इज़राइल को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। गाजा में जनसंहार के बीच मोदी सरकार कमजोर और अस्पष्ट भाषा में युद्धविराम व मानवीय सहायता की बातें करती रही हैं। भारतीय कंपनियों ने, सरकार की सहमति से इज़राइल को 900 हर्मीस (Hermes) ड्रोन और गोला-बारूद उपलब्ध कराया। इज़राइलके निर्माण क्षेत्र में फ़िलिस्तीनी श्रमिकों की जगह लेने के लिए हजारों भारतीय मज़दूरों को भेजे (रामचंद्रन 2024; मार्सी 2024; इंडियन एक्सप्रेस 2025) ।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से पिछली गैर-भाजपा सरकारें भी अमेरिका के साथ संबंध मज़बूत करने की कोशिश की है। इसके लिए वहाँ के भारतीय प्रवासी समुदाय पर निर्भर रहने की कोशिश करती रही हैं। इज़राइल-अमेरिका संबंध लंबे समय से घनिष्ठ रहे हैं अमेरिका से अपने सम्बन्ध को अच्छा करने के लिए, इज़राइल को एक माध्यम के रूप में देखा है। मोदी सरकार ने अपने हिंदुत्ववादी संगठनों के ज़रिये (जिनकी शाखाएँ अमेरिका और ब्रिटेन में भी हैं) इस दिशा में और अधिक प्रयास और संसाधन लगाए हैं। अमेरिका में हिंदू राष्ट्रवादी लॉबी समूहों की वृद्धि और प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक रहा। एआईपीएसी (अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमिटी) और हिन्दू अमेरिकन फाउन्डेशन (HAF) को कई समूहों के लिए आदर्श मॉडल माना गया। इनके संबंध एआईपीएसी और अमेरिकन ज्यूइश कमिटी (एजेसी) से और गहरे हुए हैं। जिन्हें मोदी सरकार और इज़राइल, दोनों ने कैपिटल हिल की राजनीतिक छत्रछाया में प्रोत्साहित किया है, जो समय के साथ अधिक रूढ़िवादी और इस्लामोफोबिक होता गया है (कॉकबर्न Cockburn 2024)।13
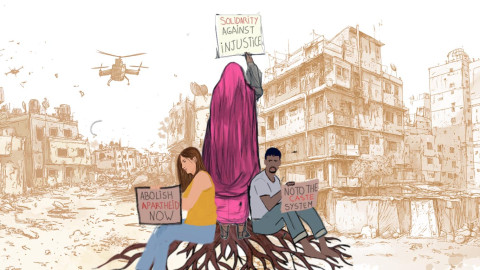
Illustration by Fourate Chahal El Rekaby
अब क्या?
शीत युद्ध का अचानक अंत एक बड़ा वैश्विक मोड़ था। इसके साथ साम्यवादी गुट का पतन हुआ और उन देशों का रूप बदल गया जो पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर गए। इन देशों में राज्य का नियंत्रण और मार्गदर्शन का स्तर अलग-अलग रहे। 1990 के दशक से अब तक दुनिया भर में अनेक सरकारें इज़राइल के साथ लगातार बढ़ते समायोजन की ओर रहीं। वहीं तेल अवीव ने (शब्दों और भावनाओं दोनों में) ओस्लो और बाद के समझौतों के तहत अपना दायित्व निभाने की जगह धोखा दिया। ग़ाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी खुले जेल में बदल दिया गया। पश्चिमी तट पर बस्तियाँ बनाई गईं। फ़तह नेतृत्व और पीए की सुरक्षा संरचना को अवैध कब्ज़े का उप-ठेकेदार बना दिया गया और पीए की आर्थिक पुनरुत्पत्ति को पश्चिमी अनुदान पर निर्भर कर दिया गया।
इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य देशों और कुछ मध्य-पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों में जहाँ तानाशाही या राजशाही शासन लंबे समय तक बना रहा, इज़राइल के ‘प्रबंधन’ (अर्थात् कब्ज़े वाले क्षेत्रों में उसके क्रूर नियंत्रण और विस्तार) को रोकने में बहुत कम काम किया गया। ईरान-नेतृत्व वाले ‘प्रतिरोध धुरी’ को छोड़ कर, नागरिक समाज में फ़िलिस्तीन के समर्थन की आवाज़ें बढ़ीं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका (ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका) में देखने को मिली। विशेषकर दक्षिण अफ़्रीका में जिसने अपने नस्लवादी अतीत पर काबू पाया।
तो भारत में कहानी क्या है? ऊपर पहले ही कहा गया कि भारत में ग़ाज़ा और पश्चिमी तट के फ़िलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने वाले नागरिक विरोध अन्य लोकतांत्रिक देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर रहे हैं। यदि आगे का रास्ता निर्धारित करना है और सकारात्मक दिशा में बढ़ना है, तो हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ ताकि हम इसे बदल सकें। इस कहानी का एक हिस्सा हिंदुत्व सरकार और उसकी निगरानी करने वाले समूहों द्वारा दमन और कानूनी कार्रवाइयाँ में निहित है। ये समूह घृणास्पद सामाजिक ट्रोलिंग करते हैं, मिलीभगत वाली पुलिस और निचली अदालतों के साथ झूठे मामले दर्ज कराते हैं और कभी-कभी ‘देश-द्रोही’ कह कर शारीरिक हमले भी करवाते हैं (गुंगोर 2024)। कहानी का दूसरा हिस्सा भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक चरित्र में निहित है।
भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग 1.4 अरब है, पर कामकाजी आबादी लगभग 64 करोड़ है। इनमें से आधे से अधिक लोग प्राथमिक कृषि/मत्स्य पालन/खनन जैसे सेक्टरों क्षेत्रों से जुड़े हैं। केवल लगभग सात प्रतिशत लोग औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित वेतन, भुगतान के साथ छुट्टी, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की कुछ हद तक सुरक्षा होती है। बाकी सभी अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ औपचारिक क्षेत्र की कोई सुरक्षा नहीं है, वेतन कम है और यूनियन बनाने का औपचारिक अधिकार भी सीमित है (तेहलका 2022)। अनुमानतः केवल तीन प्रतिशत कामगार ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़ा है। इनका भारी हिस्सा बड़े यूनियनों से जुड़ा है और वे अलग-अलग राजनीतिक दलों के नियंत्रण में आते हैं। आज सबसे बड़ा यूनियन भाजपा के प्रभाव में है, उसके बाद कांग्रेस और फिर वामपंथी व क्षेत्रीय दलों के अधीन यूनियनों आते हैं। इसका मतलब यह रहा है लंबे समय से आम जनता का बड़ा हिस्सा रोज़गार, रोज़मर्रा के जीविकोपार्जन और बुनियादी स्वतंत्रताओं से जुड़ी समस्याओं में उलझा रहा है।
यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियों से स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का फोकस उन विकास नीतियों पर रहा है जिन्होंने आर्थिक पीड़ा पहुंचाई है, कुछ विशेष स्वतंत्रताओं के उल्लंघन और सामाजिक तथा क्षेत्रीय भेदभाव पर। आम लोगों के लिए विदेश नीति के मुद्दे घरेलू चिंताओं की तुलना में दूर की कौड़ी लगते हैं। इसलिए वे ज़्यादातर उन्हीं संस्थाओं की बातें सुनते हैं जिनसे वे जुड़े हैं। चाहे वे राजनीतिक दल हों, ट्रेड यूनियन हों या सामाजिक-धार्मिक निकाय हों जो उन्हें भावनात्मक या कुछ हद तक भौतिक सहारा देते हैं।
संदेश साधारण है। अब तक भारत में फ़िलिस्तीन समर्थक विरोध और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन बहुत छिटपुट रहे हैं। ये मुख्य रूप से महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और कभी-कभार अन्य शहरी केन्द्रों तक सीमित रहे हैं। ये रैलियाँ प्रायः मुख्यधारा की संसदीय वाम पार्टियों द्वारा आयोजित की जाती हैं, जो लोगों की भागीदारी के लिए अपनी ट्रेड यूनियनों और छात्र संगठनों पर निर्भर रहती हैं। मुस्लिम राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और मुस्लिम छात्र संगठन भी कभी-कभी सार्वजनिक रूप से एकजुटता व्यक्त करते हैं, पर वे फ़िलिस्तीन मुद्दे को अक्सर धार्मिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं न कि सार्वभौमिक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से।14 अपेक्षाकृत स्वाभाविक रूप से, जहाँ बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय फ़िलिस्तीनियों की पीड़ा के साथ गहरी आत्मीयता महसूस करता है, वह है कश्मीर घाटी, जहाँ दशकों से भारी भारतीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद इज़राइली हमलों के खिलाफ कश्मीर की कई मस्जिदों में सामूहिक नमाज़ें और विरोध हुए (ज़र्गर 2023)। बाद में आधिकारिक तौर पर अधिकारियों ने कश्मीर में फ़िलिस्तीन समर्थन में लगभग सभी तरह के जलसों पर रोक लगा दी और यहाँ तक कि मौलवियों को चेतावनी दी कि वे अपने उपदेशों में फ़िलिस्तीन का ज़िक्र न करें। इसके बावजूद मार्च और जून 2025 में वहाँ एकजुटता की कुछ कार्यवाहियाँ फिर उभरीं (यूसुफ़ 2025; द वायर 2025)।15
पश्चिम की तुलना में, भारत में धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक नियंत्रण से स्वतंत्र संगठनों द्वारा आयोजित फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकजुटताएँ नहीं रहीं हैं। पश्चिमी उदार लोकतंत्रों में यह आंदोलन अपेक्षाकृत आरामदायक मध्य वर्ग में अधिक दिखाई देता है। ऐसा मध्य वर्ग जो रोज़गार की बुनियादी चिंताओं से कुछ हद तक मुक्त होता है और विदेश नीति पर अधिक ध्यान दे सकता है। भारतीय मध्य वर्ग, जो पिछले दो दशकों में बढ़ा है, जिसका राजनीतिक रूख प्रगतिशीलता की तुलना में अधिक प्रतिक्रियावादी और संकुचित रहा है। यही कारण है कि भाजपा और हिंदुत्व का समर्थन केवल अभिजात वर्ग में ही नहीं बल्कि मध्य वर्ग की ऊपरी, मध्य और निचली परतों में भी तेज़ी से बढ़ा है।
फिर भी, इस मध्य वर्ग में प्रगतिशील हिस्से मौजूद हैं और उनकी संख्या बढ़ी है। सोशल मीडिया ने युवाओं में दुनिया और फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, इसकी जागरूकता बढ़ाई है। यह प्रगतिशील हिस्सा, खासकर युवा, वामपंथी पार्टियों और छोटे-छोटे गुटों (जिनकी संख्या, भारत के भौगोलिक आकार को देखते हुए, बहुत अधिक है) के साथ सामाजिक-राजनीतिक आधार पर जुड़ रहे हैं। वे अनेक प्रगतिशील कारणों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन वंचित समूहों के साथ प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं जो आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर हैं। परिणामस्वरूप, पूरे देश में विभिन्न फ़िलिस्तीन एकजुटता समूह उभर आए हैं।
इनमें से कुछ समूह मौजूदा सांस्कृतिक, राजनीतिक या (मुस्लिम) धार्मिक निकायों से जुड़े हैं। अन्य स्वतंत्र और प्रगतिशील समूह हैं जो आम तौर पर हिंदुत्व और मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। ये बड़े वाम दलों के महिला, छात्र और यूनियन संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और सैकड़ों से हजारों की संख्या में एकत्र हो पाते हैं।16 वे स्वतंत्र कार्यवाहियाँ भी करते हैं और कभी-कभी सामान विचारधारा वाले संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाते हैं। इन समूहों ने सोशल मीडिया पर अंग्रेज़ी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी, विश्लेषण और वीडियो साझा किए हैं। उन्होंने छोटे स्तर पर सड़कों और मुहल्ले में पर्चे बाँटे जो आमतौर पर प्रायः गैर-भाजपा शासित राज्यों में।
फिर भी, इन रैलियों में भी अक्सर अचानक ‘फ़्लैश’ विरोध होते हैं, किसी भीड़भाड़ वाले बाज़ार या चौराहे पर जमा होकर, और पुलिस आने से पहले हट जाते हैं। मई से मध्य जुलाई 2025 के बीच, मैकडॉनल्ड्स और डॉमिनोज़ पिज़्ज़ा के कुछ आउटलेट्स को बहिष्कार करना, विनिवेश और प्रतिबंध (BDS) लगाने की मांग की गई। ये विरोध प्रदर्शन हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और अन्य शहरों में देखी गईं। उल्लेखनीय है ‘इंडियन डांसर्स फॉर ग़ाज़ा’ज़ चिल्ड्रन’ (IDGC) का गठन, जो अपने प्रदर्शनों के माध्यमों से मानवीय सहायता के लिए धन जुटाता है और ग़ाज़ा के प्रिंसेस बसमा सेंटर से जुड़ा है, जो विकलांग बच्चों के लिए काम करता है। यह सब नया है और संकेत है कि फ़िलिस्तीन का प्रश्न विशेषकर युवाओं की बीच कल्पना से अधिक जगह बना रहा है।17 यह अभी भी भारतीयराज्य के विरुद्ध एक कठिन लड़ाई है, लेकिन आगे बढ़ रहा है।
तो आगे का रास्ता क्या है? लगभग सभी सरकारें आधिकारिक तौर पर कहती हैं कि वे इज़राइल–फ़िलिस्तीन विवाद का हल दो-राज्य समाधान में देखती हैं। यह लंबे समय से एक सुविधाजनक मुखौटा बन गया है, जिससे सरकारें अपनी विफलताओं और किसी ठोस काम करने की अनिच्छा को छुपा लेती हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो या सामूहिक रूप से।
ग़ाज़ा के संदर्भ को छोड़ दें, तो पश्चिमी तट पर इज़राइली बस्तियों का विस्तार और सशस्त्र हस्तक्षेप जो अक्सर फ़तह की अनुमति या कभी-कभी मिलीभगत से होता है, फ़िलिस्तीनियों को एक टुकड़ा (एक बंटुस्तान) मिलने की संभावना को लगभग खत्म कर दिया है। वे टुकड़े भी यदि मिले तो संसाधन-विहीन होंगे। सभी अवैध यहूदी बस्तियों (जिन्हें वे यहूदा और सामरिया कहते हैं) को हटाने के लिए इज़राइल से कहना, ऐसा मांगना है मानो वह गृहयुद्ध का जोखिम उठाए। असल में, 2023 में हुए हमास के हमले ने इज़राइली दक्षिणपंथी और अतिदक्षिणपंथी, और कुछ मध्यमार्गी राजनेताओं के लिए बहाना उपलब्ध करा दिया है की वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए इसको ‘अंतिम समाधान’ के रूप में पेश कर रहे हैं जिसको अब संगठित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
हमें यह मानना होगा कि यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, पर अभी इसे तेज़ कर दिया गया है। ग़ाज़ा में इसका अर्थ है ग़ाज़ा पट्टी के उत्तरी हिस्से या उसका बड़ा भाग क्षेत्रीय रूप से कब्ज़े में लेना। इसका नतीजा भूखमरी, कुपोषण, बीमारी, सैन्य हमले से जनसंख्या को कम करना और आगे विस्थापन के ज़रिये दक्षिणी इलाक़ों की सीमित हिस्सों में और भी बदतर जेल जैसी परिस्थितियाँ बनाना होगा। उद्देश्य है अधिकांश, या यदि संभव हो तो सभी लोगों के लिए जीवन असहनीय कर देना।
नवीनतम योजना यह है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को बाहर रखा जाए और केवल कुछ चुनिंदा वितरण केन्द्रों पर न्यूनतम सहायता दी जाए। इस योजना का उद्देश्य ग़ाज़ावासियों की भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं है। असल नीयत यह है कि इज़राइल के सहयोगियों को शांत रखा जाए ताकि वे ‘बेहतर अंतरात्मा’ के साथ चुप रहे, जबकि जातीय सफ़ाए की प्रक्रिया जारी रहे। इस तरह स्थितियाँ इस क़दर बनी रहें कि ग़ाज़ावासी और अधिक ‘स्वैच्छिक पलायन’ का विकल्प चुनें और दुसरे देशों में बस जाएँ।
यहाँ ट्रंप प्रशासन भी अपनी भूमिका निभा रहा है और कई देशों जैसे- सूडान, सोमालिया, सोमालीलैंड (विभाजित क्षेत्र), लीबिया, इंडोनेशिया आदि से संपर्क कर रहा है संभवतः इन्हें वित्तीय और दूसरे प्रलोभन दिए जा रहे हैं। पश्चिमी तट में अवैध बस्तियाँ और अधिक बढ़ाई जाएँगी और फ़िलिस्तीनियों पर नियंत्रण का ;प्रबंधन’ करने के लिए उनके नेताओं पर दमन और रिश्वतखोरी की रणनीतियां तेज की जाएगी। तेल अवीव और वॉशिंगटन के लिए ‘जोर्डन विकल्प’ का एक विशेष संस्करण भी विचार के लिए है। इसका मतलब यह होगा कि उनके शासकों के लिये डंडा और गाजर की समान रणनीति लागू करके जोर्डन को आंशिक रूप से या पूरी तरह फ़िलिस्तीनियों की नई बसावट के रूप में तैयार किया जाए। संक्षेप में, यह सब उस योजना का हिस्सा है जिसमें शासकों को खरीदकर या दबाकर वेस्ट बैंक के लोगों को बाहर भेज देना शामिल है। फिर भी, चाहे योजनाएँ कितनी भी चालाकी से बुनी जाएँ, गाज़ा और वेस्ट बैंक दोनों के लिए इन इज़रायली महत्वाकांक्षाओं के बीच अभिलाषा और वास्तविकता के बीच एक विशाल खाई मौजूद है — इरादा बड़ा है, पर हक़ीक़त उसे पूरा होने नहीं दे रही।
नस्लभेदी व्यवस्था (अपार्थाइड ) पर ध्यान केंद्रित करें
इस इस्राइली परियोजना को पूरी तरह निष्फल करने के लिए प्रमुख प्रश्न यह है कि राजनीतिक ताकतों और सत्ता के संबंधों को किस तरह बदला जाए ताकि वे फिलिस्तीनी संघर्ष के पक्ष में और इस्राइल के खिलाफ खड़े हों? शुरुआत में ध्यान अंतिम लक्ष्य पर नहीं होना चाहिए, चाहे वह दो-राष्ट्र समाधान हो या एक-राष्ट्र समाधान, यह निर्णय फिलिस्तीनियों पर छोड़ा जाना चाहिए। हालाँकि, राजनीतिक दबाव को इस्राइल के उस चरित्र पर केंद्रित होना चाहिए, जो दुनिया का एकमात्र उपनिवेशवादी-बसाहट और अपार्थाइड राज्य है। इस्राइल गैर-यहूदियों और इस्राइल के भीतर फिलिस्तीनियों को समान अधिकारों से वंचित करता है। वह, अवैध क़ब्ज़ेदार होते हुए भी, उन अधिकारों से इनकार करता है जो अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार कब्ज़े में रखे गए लोगों को मिलने चाहिए। साथ ही वह उन फिलिस्तीनी परिवारों और उनके वंशजों के वापसी के अधिकार से भी इनकार करता है जिन्हें अतीत में जबरन विस्थापित किया गया था, और जिसे स्वीकार करना इस्राइल की संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने की औपचारिक शर्त थी। समानता, अधिकार, न्याय और लोकतंत्र का विमर्श तीन महत्वपूर्ण संघर्ष क्षेत्रों को एकीकृत करने का एक माध्यम बन जाता है, और भारतीय संदर्भ में, अपार्थाइड पर ध्यान एक व्यापक आधार को आकर्षित करता है।
इसराइल की बस्तिवासी-औपनिवेशिक और अपार्थाइड प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करना यह संभावना भी खोलता है कि उन फ़िलिस्तीनियों के बारे में बात की जा सके जो इसराइल के भीतर द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, और उस फ़िलिस्तीनी प्रवासी समुदाय के बारे में भी, जो जनता और सरकारों, विशेषकर पश्चिम में अपने बढ़ते प्रभाव के कारण एक अधिक महत्वपूर्ण बाहरी समर्थन स्रोत बन गया है। लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष यह भी अनुमति देता है कि वार्ता में पड़ोसी अरब देशों को शामिल किया जा सके, जो अधिकांशतः किसी न किसी प्रकार की तानाशाही के अधीन पीड़ित बने रहते हैं। प्रगतिशील प्रगति और सफल प्रतिरोधों के बीच एक पारस्परिक और प्रतिपुष्टि संबंध है, चाहे वे अधिकृत क्षेत्रों (OTs) में घटित हों या अरब दुनिया में।
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के शासक निरंकुशतंत्रों के लिए इन विकासों से डरने का कारण इस्राइल से भी अधिक है। यदि इनमें से किसी एक तानाशाही का पतन हो और उसकी जगह एक स्थिर और दीर्घकालिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, तो संपूर्ण क्षेत्रीय और यहाँ तक कि वैश्विक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। यह फिलिस्तीनी संघर्ष को एक गंभीर प्रोत्साहन देगा, अन्य तानाशाहियों पर वास्तविक डोमिनो प्रभाव डालेगा, और प्रमुख बाहरी शक्तियों को मौजूदा गठबंधनों और उनके पीछे की सोच का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करेगा। इस क्षेत्र में एक स्थिर लोकतांत्रिक शासन अभी आना बाकी है, लेकिन यह निश्चित है कि अरब विद्रोहों का पहला और दूसरा चरण (प्रारंभिक 2010 का दशक और 2018-2024) एक तीसरा विद्रोह अवश्य आएगा, जिसमें फिर से सबसे अधिक वांछित परिवर्तन हासिल करने की संभावना होगी।
इस कहावत में अब भी बहुत सच्चाई है कि येरुशलम (अर्थात् फिलिस्तीन की मुक्ति और न्याय) का रास्ता काहिरा और अम्मान से होकर गुजर सकता है! जहाँ तक विभिन्न फिलिस्तीनी गुटों के बीच उद्देश्य और व्यवहार की अधिक एकता का प्रश्न है, और फिलिस्तीनी जनता के प्रति उनके नेतृत्व की अधिक लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है तो आशा की जानी चाहिए कि मार्च 2025 में किया गया वादा पूरा होगा: फिलिस्तीनी विधान परिषद और फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) के नए राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। इसके अलावा, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद (जो पीएलओ की विश्व संसद है, जिसमें सभी फिलिस्तीनी राजनीतिक समूह शामिल हैं और जिसके 700 से अधिक प्रतिनिधि हैं) की भी जल्द बैठक हो। इसकी अंतिम बैठक 2018 में हुई थी, और यही परिषद पीएलओ की कार्यकारी समिति का चुनाव करती है। फिलिस्तीनी जनता इससे कम की हकदार नहीं है।18
चाहे यह रणनीतिक बदलाव कभी हो या न हो, भारत में एकजुटता कार्य को मजबूत करने का मार्ग स्पष्ट है। इस्राइल आज दुनिया का एकमात्र शेष उपनिवेशवादी-अपार्थाइड राज्य है। भारत की सभी पार्टियाँ जिनमें भाजपा के हिंदुत्व-प्रेरित पूर्ववर्ती जनसंघ भी शामिल है, दक्षिण अफ्रीकी अपार्थाइड के खिलाफ थीं और उन्होंने उन सभी भारतीय सरकारों के रुख का समर्थन किया था जिन्होंने इसके खिलाफ पूर्ण राजनयिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, खेल प्रतिबंध लगाए थे। यह एक इतिहास है जिसे अब वर्तमान सरकार और हिंदुत्व संगठनों के व्यापक समूह के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि मुख्यधारा की भारतीय वामपंथी पार्टियों ने इस तथ्य को अधिक उजागर नहीं किया है।19 अपनी अपेक्षाकृत बड़ी संख्या और संसाधनों के कारण ये पार्टियाँ समय-समय पर फिलिस्तीन के समर्थन में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों की अग्रिम पंक्ति में रही हैं। लेकिन वे अभी तक, जारी जनसंहार के बावजूद, इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि भारत अपने राजनयिक संबंध अपार्थाइड इसराइल के साथ तोड़ दे और हथियारों पर प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंध लगाएं, जिसमें सभी भारतीय प्रवासी श्रमिकों की वापसी की मांग भी शामिल हो।
बेशक, यह भारतीय सरकार यह कदम नहीं उठाएगी, और बीजेपी के विरोधी राजनीतिक पार्टियाँ भी इस मांग में शामिल नहीं होंगी। लेकिन यह रुख अब लेना ज़रूरी है, ताकि अधिक से अधिक जनता का दिल और दिमाग जीतने का प्रयास किया जा सके। नई दिल्ली पर पीछे हटने का दबाव डाला जा सके और घरेलू स्तर पर वाम राजनीति के लिए एक व्यापक समर्थन और आधार तैयार किया जा सके।
यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस हिंदुत्व-प्रेरित सरकार और ज़ायोनी इस्राइल के बीच महत्वपूर्ण समानताएँ मौजूद हैं। इस्राइल एक अपार्थाइड राज्य है, न कि लोकतंत्र या ‘जातीयतंत्र’। मोदी के अधीन भारत अभी पूरी तरह ऐसा नहीं है, लेकिन यह तेजी से एक अपार्थाइड राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है (वनाइक, 2022)। हालाँकि, इस्राइल और बस्तियों में अधिकांश यहूदियों की स्थिति अधिकांश भारतीयों से अलग है। वे उतने गरीब या भौतिक रूप से असुरक्षित नहीं हैं जितने अधिकांश हिंदू। भारत में घृणित जाति व्यवस्था है, जो मुख्यतः (लेकिन केवल) हिंदुओं को प्रभावित करती है। भारत में रोज़मर्रा की हिंसा और नियमित भ्रष्टाचार कहीं अधिक है, और वर्ग तथा जाति की शक्ति लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करती है तथा क़ानून में हेरफेर करती है, जिससे गरीबों को नुकसान पहुँचता है। यह सब इस्राइल में यहूदियों के बीच मौजूद नस्लीय भेदभाव और असमान शक्ति संबंधों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है।
उन संगठनों और आंदोलनों के लिए, जो विशेष रूप से फिलिस्तीन के साथ एकजुटता को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहे हैं, उनके लिए सबक स्पष्ट है। उन्हें उन अन्य ताकतों से जुड़ना चाहिए जो हिंदुत्व का राजनीतिक-लोकतांत्रिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर विरोध कर रही हैं। यानी, भारत में फिलिस्तीनी मुद्दे को आगे बढ़ाने में सफल होने के लिए केवल एकजुटता पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। यह व्यापक मानवीय और संस्थागत सहानुभूति और समर्थन का क्षेत्र बनाने का भी साधन है।
ऐसे दृष्टिकोण का व्यावहारिक अर्थ क्या होगा? भारत में कई संगठन हैं जो नागरिक स्वतंत्रताओं और जनता की आजीविका की रक्षा में सक्रिय हैं। इनमें वे संस्थाएँ भी शामिल हैं जो क्षेत्रीय सीमाओं के परे और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) शामिल है, जिसने अब इस्राइली नरसंहार का मुद्दा उठाया है। इसी तरह नेशनल एलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (NAPM) है, जो तीन दशक पुराना विभिन्न लोकप्रिय और प्रगतिशील संघर्षों का नेटवर्क है।
भारतीय सरकार की निराशा और गुस्से के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने बार-बार पुष्टि की है कि जाति नस्ल सम्मेलन के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह वंश और पेशे के आधार पर आधारित संस्थागत भेदभाव का एक रूप है। जबकि भारतीय संविधान ‘अछूत प्रथा’ को प्रतिबंधित करता है, यह स्वयं जाति व्यवस्था को अवैध नहीं ठहराता। यहाँ फिर एक अवसर है, जहाँ फिलिस्तीन के साथ एकजुटता का कार्य केवल इस्लामोफ़ोबिया से लड़ने वाली ताकतों के साथ ही नहीं, बल्कि दलितों, अन्य निचली जातियों और स्वयं जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले समूहों के साथ भी जुड़ सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि भारत की नवउदारवादी कृषि और खनन नीतियाँ कॉर्पोरेट कृषि की खोज में मध्यम और छोटे किसानों को विस्थापित कर रही हैं, साथ ही मध्य भारत के वन पट्टी और उत्तर-पूर्व में आदिवासी आबादी को भी।
कृषि में इस्राइली तकनीकी सहयोग और उसका सैन्य ज्ञान, भारत में मौजूदा वर्ग संबंधों को देखते हुए, संभावना है कि इस कॉरपोरेटिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। उसकी सैन्य और साइबर निगरानी क्षमता और उपकरण अपने-अपने तरीक़े से इस तरह के जबरन विस्थापन के विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए और भी आवश्यक है कि इतने सारे भारतीयों और फिलिस्तीनियों द्वारा झेली जा रही समानताओं के पैटर्न को पहचाना जाए। इन सामूहिक एकजुटताओं का निर्माण देश के भीतर होना चाहिए। यह विदेशी फिलिस्तीनी एकजुटता समूहों और नेटवर्कों के साथ संबंध बनाने, सूचनाओं के आदान-प्रदान और साझा बयानों व कार्य कार्यक्रमों की तैयारी के लिए चल रहे प्रयासों को और भी मज़बूती देगा।
करने के लिए बहुत कुछ है — और हमें तुरंत इसमें लग जाना चाहिए!
इस लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे टीएनआई के विचारों या स्थिति को प्रतिबिंबित करें।
Palestine Liberation series
View series-
भारत, इज़रायल, फ़िलिस्तीन नए समीकरण नई एकजुटताओं की मांग करते हैं
Publication date:
